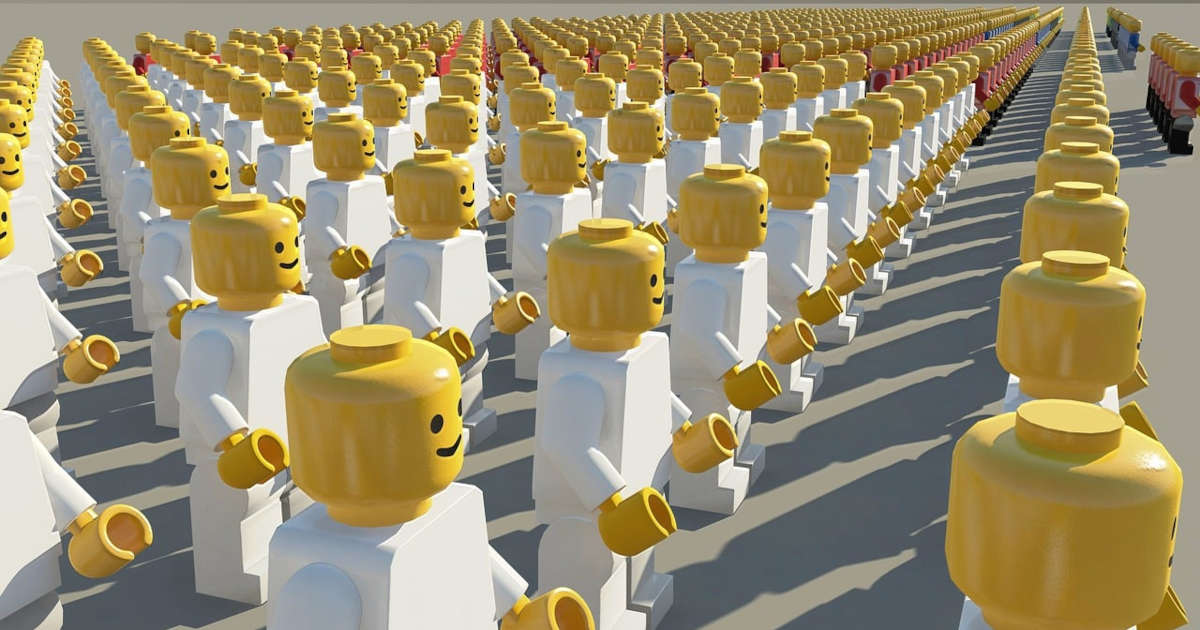आपको शीर्षक पढ़कर आश्चर्य हो, पर अब यह पूछना कि, “क्या लोकतंत्र दरक रहे हैं?” बेमानी हो चुका है, महत्वपूर्ण हो उठा है यह प्रश्न की लोकतंत्र क्यों दरक रहे हैं। गौर करने की बात है कि यह किसी ईक्के दुक्के देश नहीं, दुनिया के कई देशों में हो रहा है जहां दक्षिणपंथी एकनायकतंत्र अपनी जडें जमा रहा है। कहीं कोई बोल्सेनारो, कोई इरदुगान, या कोई देश, हंगेरी या अर्जेंतिना। फ्रांस अबतक इस संभावना से बचा हुआ है – लोकतंत्र की जड़ें शायद वहां गहरी हैं। पर मरीन ले पेन की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर सवाल उठता है कि क्या फ्रांस 2027 में खैर मना पायेगा? हाल की बात देखें तो हॉलेंड भी इस बदलाव की चपेट में आ चुका है और इटली भी। अमेरिका पिछले चुनावों में इस परिणाम से बमुश्किल बच पाया - वहां भी लोकतंत्र की जड़ें अभी इतनी गहरी हैं, की व्यवस्था द्वारा नियुक्त एक राजनैतिक प्राधिकारी भी किसी उतावले अधिनायक के सामने अड़कर उसे स्पष्ट शब्दों में सुना सकता है कि चुनावी प्रक्रिया में कोई खोट नहीं थी। उस एक दृढ़ता ने ही सारी बिसात पलट दी। इसके विपरीत, कई जगहों पर तो संवैधानिक पदों पर बैठे महानुभावों को सत्ता के सामने, झुकते, बिछते लाचार होते देखा जा सकता है – चाहे वह डर के बहाने हो या लालच की वजह से।
भारत में भी दक्षिणपंथी अधिनायकवाद की तरफ यह रुझान शीघ्रता से जड़ें जमा रहा है। कई लोग इसका श्रेय, तो कई लोग इसका दोष, मोदी-शाह जोड़ी को दे रहे हैं। पर गंभीरता से देखा जाये, तो हमें ऐसे सतही, व्यक्ति-केंद्रित विश्लेषणों से कहीं आगे की सोचने की जरुरत है। जिस प्रक्रिया की हम बात कर रहे हैं, उसमें व्यक्ति विशेष बेमानी हैं प्रक्रिया ज्यादा महत्वपूर्ण है। गीता की भाषा में कहा जाये तो नेता विशेष महज एक ‘निमित्त’ होते हैं। वे संयोगवश उस प्रक्रिया को गति प्रदान देते हैं जो उनके बजाय भी अपनी राह पर कायम रहती है, शायद थोड़ी कम रफ्तार से, पर दिशा अवश्य ही वही रहती है। गौर से देखें तो वर्तमान व्यवस्था उन्हीं बबूलों की फसल काट रही है, जिन्हें बोया काँग्रेस ने था! अतः यह जरुरी है कि हम उन ताकतों को चिन्हित करें जो अलग अलग राष्ट्रों को दक्षिणपंथी अधिनायकवाद की दिशा में ढ़केल रही हैं। उन ताकतों में धनकुबेर बनने की जल्दबाजी, लोकतंत्र के प्रति अनास्था, और समता, मानवाधिकार या तत्सम किसी भी उदारवादी नितियों और संस्थाओँ के प्रति हेय दृष्टि सहज नजर आ जाती है।
लोकतंत्र के प्रति यह अनास्था या असहिष्णुता कोई रातोंरात की उपज नहीं है। यह प्रक्रिया कई वर्षों से आकार ले रही थी। पर इस सदी के पहले दशक के समाप्त होते होते इसने रफ्तार पकड़ी है। थॉमस फ्रीडमॅन ने अपनी किताब ‘थँक्यू फॉर कमिंग लेट’ में 2007-08 को जैविक, इलेक्ट्रॉनिक और संचार की विभिन्न टेक्नॉलॉजियों के संधिस्थल के रूप में चिन्हित किया है जहां से धन-संचय के नये-नये अवसरों को जुंबिश मिली और पूंजी ने फिर मुड़कर पीछे नहीं देखा। नये युग की टेक्नॉलॉजी, खासकर सूचना की टेक्नॉलॉजी ने धन, या यों कहें, संसाधन संचय के ऐसे अवसर उपलब्ध किये हैं, कि गाफा (गूगल, ऍपल, फेसबुक और अमॅझॉन) जैसी बड़ी कंपनियां अपने संसाधन-बल के बूते पर अगर चाहें तो कई राष्ट्रों तक से भिड़ सकती हैं।
नये युग का यह संचय-लोलुप पूंजीवाद इतना उग्र, आक्रामक और अधीर है कि अब उसे लोकतंत्र एक बोझ सा लगने लगा है। पूंजी संचय पर नियंत्रण और संतुलन रखने की सारी व्यवस्थाएं इसे अपनी राह के रोड़ों की तरह महसूस होने लगी हैं जिनपर काबू पाना जरूरी है। और इसके लिये जरूरी हुआ तो काबू लोकतंत्र पर पाना भी है, जहां नागरिक और अन्य संस्थाएं बहुत ज्यादा सवाल पूछती हैं। नये, आक्रामक पूंजीवाद को अब प्रश्न पूछनेवाले नागरिक नहीं, आज्ञापालक प्रजा चाहिये जो उनकी पसंद की उपभोक्ता भी बनी रहे। संसदीय लोकतंत्र ऐसी आज्ञापालक प्रजा और संस्थाएं उपलब्ध नहीं कराता, सो पूंजी के लिये लोकतंत्र के विकल्प खोजना अब जरूरी हो गया है।
पर चक्कर यह है कि ये धनकुबेर, आप उन्हें अलग अलग नामों से पुकार सकते हैं; कॉर्पोरेट, गोदी सेठ, नवधनाढ्य या और कुछ, यह खुद, प्रत्यक्ष रूप से, नागरिकों पर हुकुमत नहीं चला सकते। निरीह प्रजा भी ऐसी व्यवस्था को स्वीकार नहीं करेगी। अतः पूंजी को ऐसी शासन प्रणाली की आवश्यकता है जो नागरिकों पर नियंत्रण रख सके। चूंकि उदारवादी लोकतंत्र के मूल्य ऐसे नियंत्रण के ठीक विपरीत हैं, पूंजी को अब आवश्यकता है दक्षिणपंथी अधिनायकवाद की या फिर, आवश्यक हुआ, तो तानाशाही की। अब वो दिन लद गये जब सामंतवाद पर काबू पाने के लिये पूंजी को लोकतंत्र की जरूरत थी। पूंजी को अब जरूरत है, बाहुबली अधिनायकवाद की जो आंतरिक या बाहरी सुरक्षा की दुहाई देकर आज्ञापालक प्रजा और नतमस्तक संस्थाएं मुहय्या कराए। संयोग कहें या दुर्भाग्य, महामारी भी ऐसे समय आयी और कार्यपालिका ने महामारी की आड़ में नागरिकों को ऐसे साधा, कि वह मनमाने आदेशों को भी कोई प्रश्न किये बिना मान लेने की आदत ड़ाल बैठे हैं। महामारी खत्म हो गयी पर यह आदत बरकरार रही और रखी गयी, और कई मनमाने आदेश भी कायम रहे। कार्यपालिका ने इस नये हथियार के सहारे सुनिश्चित कर लिया की सड़कें वीरान रहें और, डॉ। लोहिया के शब्दों में कहें तो ‘संसद आवारा’।
पर यह सब अचानक, रातोंरात नहीं हो जाता। इसके पीछे एक सुनियोजित प्रयत्न होता है, भूमिका बांधने का और माहौल बनाने का। और यह काम किया जाता है मिड़िया के माध्यम से और प्रचार के हथियार से। इस माहौल बनाने के प्रॉजेक्ट के तहत लोकतंत्र के दोषों को बढ़ाचढ़ाकर गिनाना, वर्दी और अनुशासन का बढ़ता महिमामंड़न, वर्तमान व्यवस्था पर दोषारोपण जैसे सारे हथकंड़े शामिल हैं। बात यहीं पर नहीं रूकती। माहौल बनाने के लिये एक खतरनाक ‘इतर’ का निर्माण करना भी आवश्यक हो जाता है। कहीं पर वह आतंकवादी के रूप में पेश किया जाता है तो कहीं पर घुसपैठियों के रूप में तो कहीं पर किसी धर्म या समूह विशेष के रूप में। यूरोप में मुस्लिम आप्रवासियों के खिलाफ़ बनते माहौल को इसी परिपेक्ष्य में देखा जा सकता है। फिर इसके दुष्प्रचार के दायरे में विचारघाराएं भी आने लगती हैं पहले वामपंथ के खिलाफ़, फिर मध्यमपंथ के, फिर धीरे धीरे यह हमला, पहले परोक्ष रूप से और बाद में प्रत्यक्ष रूप से सारी उदारवादी विचारधारा पर होने लगता है। इन सभी को धीरे धीरे परंपरा, समाज और राष्ट्र के लिये खतरे के रूप में चित्रित किया जाने लगता है।
जाहिर है कि ऐसे प्रचार पर प्रश्न उठें, और क्यूंकि ऐसे प्रश्न आम तौर पर छात्रों, बुद्धिजीवियों य़ा कलाकारों द्वारा उठाये जाते हैं इसलिये कोई भी अधिनायकवाद य़ा तानाशाही का यह पहला लक्ष्य होते हैं। फिर उनके खिलाफ़ दमन होता है चाहे वह पुलिस तंत्र के जरिये हो या नकाबपोश गुंड़ो के जरिये या फ़िर विश्वविद्यालय में टँक घुसाकर हो।
पर क्या ऐसा पहली बार हो रहा है? अतीत में भी, ताकतवर विचारधाराओं द्वारा ऐसे प्रयोग होते आये हैं, चाहे वह लिच्छवियों में फूट ड़ालनेवाले अमात्य वस्सकार हों, राष्ट्रपति सुकर्ण के खिलाफ़ तख्ता पलटने में भागीदार अमेरिकी खुफ़ियी तंत्र हो या फ़िर अपने देश में ही शिक्षा के क्षेत्र को शिकंजे में कसने वाले सिनेटर मॅक्कार्थी हों। शीत युद्ध के दौरान भी आपस में टकराती विचारधाराओं ने अपने देश में भी और अधीन देशों में भी यह तौर तरीके अपनाये हैं। तो अब नया क्या हो रहा है?
नया यह है कि पहले व्यवस्था परिवर्तन का काम, राज सत्ताएं करती या कराती थीं और आम तौर पर यह किसी देश विशेष तक ही सीमित रहता था। यही नहीं, इनमें व्यवहार होनेवाली प्रचार की तकनीकों का दायरा भी सीमित था। कम से कम राज सत्ताओं को तो इतना विश्वास रहता था कि यह उनके नियंत्रण से बाहर नहीं जा पायेंगी। इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण तो रूपोर्ट मर्डोक के मिड़िया साम्राज्य का है, जो अपने सारे रसूख के होते हुए भी राज-सत्ता के नियंत्रण से परे नहीं था।
पर अब का त्रिवेणी संगम एक नये ही रूप में उभरा है। इसका पहला सोपान है पूंजी और संचार की तकनीकों का एकत्रित होना जिसकी सीधी झलक हमें संचार माध्यमों की रफ़्तार और पहुँच में दिखाई देती है। इनकी वजह से अब किसी भी घटना की सूचनाएं और चित्रण पलक झपकते ही दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक जा सकती है। तत्काल संचार का यह ढ़ांचा देशों की सरहदों से परे का पहुँच रखता है। गूगल, ऍपल, फेसबुक और अमॅझॉन और अब X जैसी विश्वव्यापी संचार कंपनियां इसी संचार क्रांति की देन हैँ। अपनी तकनीकों और उपभोक्ता तक कायम की गयी पैठ ने उनके सामने मुनाफ़ा कमाने के सिमसिम को खोल दिया है।
ग्राहक के साथ संवाद के इस माध्यम का लाभ महज संचार कंपनियों तक ही सीमित नहीं है बल्कि इस माध्यम का उपयोग कर पानेवाले पूरे व्यापार जगत को है जो ग्राहक तक सीधे पहुँच सकता है और बतौर उपभोक्ता उसके व्यवहार या विचारों को भी प्रभावित करने की क्षमता रखता है क्योंकि उसके पास अब ग्राहक के बारे में अच्छी खासी जानकारी है। जितनी अधिक जानकारी, उतना ही अधिक संवाद और प्रभाव और उतना ही अधिक व्यापार और मुनाफ़ा। जानकारी अब नयी खान बन रही है या कहें तो एक समुद्र बन गया है जहाँपर “जिन खोजा तिन पाईयां गहरे पानी पैठ” वाली कहावत पूरी तौर पर लागू होती है। जो जितना गहरा पैठ पाया उसे उतना ज्यादा मिला।
पर ग्राहक के बारे में जानकारी रखने, उसके व्यवहार या विचारों को भी प्रभावित करने की जितनी ललक व्यापार को है, प्रजा के बारे में जानकारी रखने और उसके विचारों और व्यवहार को भी प्रभावित करने की ललक सरकारों को होती है। सो उन्हें भी इस नये साधन की जरूरत आन पड़ती है।
यहीं से सत्ता और पूंजी का अन्योन्याश्रय संबंध शुरु हो जाता है, पर लोकतंत्र की कीमत पर। क्यूंकि संचय लोलुप पूंजी को मुनाफ़ा ब़टोरने की जल्दी है, और अधिनायकवाद सत्ता को लोक पर नियंत्रण की, और दोनों को चाहिये जबाबदेही से छूट। इसके लिये मिड़िया और सूचनाओं पर कब्जे से बेहेतर माध्यम क्या हो सकता है?
हाल के वर्षों में प्रशासन में डिजिटल प्रणाली के उपयोग पर दिये गये जोर को भी इस परिपेक्ष में देखने की आवश्यकता है क्यूंकि अधिनायकवाद इसे बड़ी आसानी से एक निगरानी-तंत्र में बदल लेता है। बहुराष्ट्रीय पूंजी जो सिर्फ मुनाफ़े की सगी होती हैं, इसमें मददगार बन जाती हैं। सो किसी कंपनी के मुखिया को किसी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को साथ बेहिचक मंचासीन होने से कोई परहेज नही होता, ना ही कोई कंपनी जांच एजेंसी के प्रतिनिधी को अपने ऑप्स रूम में बैठाने की मांग पर खास विरोध जताती है। आखिरकार यह तो व्यवस्था के हितों की रक्षा की बात है, भले ही वह कानून की कीमत पर ही क्यों न हो। निगरानी तंत्र की यह बारीक नजर, घुटनों पर लायी गयीं नियामक संस्थाएं और स्कॉट के शब्दों में कहें तो दंड़वत लोटा हुआ नागरिक समाज; निरंकुश अधिनायकवाद को और क्या चाहिये?
यहां से संचय लोलुप पूंजी और सत्ता लोलुप शासक वर्ग की पटकथा एकाकार हो जाती है। प्रजा को अब आश्वासन दिया जाता है भौतिक सुख साधनों का, पर बदले में मांग की जाती है डिजिटल गुलामी की ताकि मुनाफ़ा अक्षुण्ण रहे। बकौल 1993 के नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री रॉबर्ट फोगेल, अश्वेतों की गुलामी भले ही नैतिक रूप से ‘जघन्य’ थी, पर आर्थिक रूप से यह ज्यादा सक्षम या एफ़िशिएंट व्यवस्था थी। वही कुतर्क अब डिजिटल युग में भी काम आ सकता है। अतः, पँडेमिक के बाद के नये युग में अधिनायक अपनी प्रजा से इतनी उम्मीद तो रख ही सकता है की वह बचे रहने के लिये एहसानमंद रहे, प्रतिरोध का स्वर ना उठाए और डिजिटल गुलामी स्वीकार करे बतौर एक सुचारू व्यवस्था के, भले ही वह नैतिक रूप से अमान्य क्यों न हो।
सुरक्षा तंत्र की मनमानी, करीने से तराशी हुई क्रूरता, उगाही का बर्ताव और प्रतिरोध के किसी भी स्वर को दबा देना, एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है जिसका उद्देश्य है नागरिकों को प्रजा में बदलना ताकि ‘मुनाफ़ा कमाने की आसानी’ सुनिश्चित की जा सके। प्रजा का काम होगा डेटा उपलब्ध करना और उसके ही आधार पर बनाये गये उत्पादों को बिना सवाल किये उपभोक्ता बनकर खरीदना। व्यापार करने की इससे बेहेतर आसानी क्या हो सकती है? सरकारों और नागरिकों का गठबंधन जो पूंजी पर नियंत्रण रख सके, अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। अब जमाना सरकारों के निगरानी तंत्र और पूंजी के बीच के गठबंधन का होगा जो नागरिकों पर नियंत्रण रख सके। जैसा मार्क एंटनी ने सीझर के वध के बाद कहा, उसी तर्ज पर गोदी पूंजी प्रजा से कहेगी ‘लोकतंत्र मर चुका है’, पर उसी सांस में नारा लगायेगी ‘लोकतंत्र अमर रहे’ !
(हंस में प्रकाशित, फरवरी 2024)
छवि सौजन्य: पिक्साबे